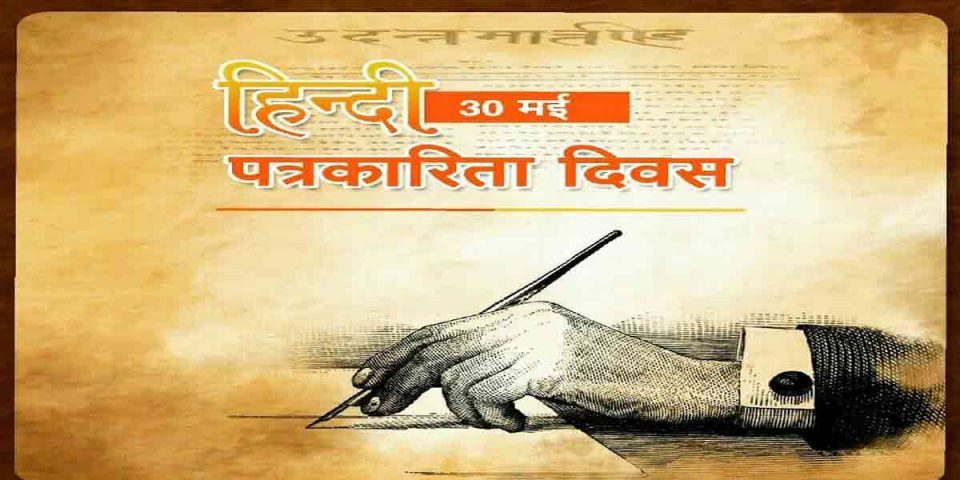अखबार शब्द का जिक्र आते ही विवेक और जवाबदेही का बिंब हमारे मन-मस्तिष्क में बनता है। यह बिंब ही अखबार की जिंदगी का उत्सकेंद्र हैं और प्राण वायु भी। प्रस्तुत है वरिष्ठ पत्रकार
उमेश चतुर्वेदी का विशेष आलेख

सामाजिक हो या राजनीतिक या फिर आर्थिक व्यवस्था, समूचे तंत्र और सोच पर कोरोना संकट का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। ऐसे में मीडिया भला कैसे अछूता रहता! कोरोना संकट ने निश्चित तौर पर अखबारों के प्रसार पर असर डाला है, लिहाजा अखबारों की कमाई भी घटी है और उनके पृष्ठ भी। इसकी वजह से एक वर्ग मानने लगा है कि अब अखबार खत्म हो जाएंगे। यह भी कहा जाने लगा है कि संकट की इस घड़ी से अखबारों का निकल पाना मुश्किल होगा, लिहाजा वे बिखर जाएंगे और हो सकता है कि आस्ट्रेलिया के विद्वान रोस डाउसन के मुताबिक अखबारों की मौत हो जाएगी…रोस डाउसन ने किस देश में अखबार की कब मौत होगी, इसका एक बाकायदा चार्ट भी तैयार किया है। हालांकि रोस डाउसन के चार्ट के मुताबिक अखबार तो नहीं मरे, लेकिन कोरोना संकट ने उनकी हालत इतनी खराब जरूर कर दी है कि अखबारों को चाहने वाला एक वर्ग भी आशंकित हो उठा है कि कहीं अखबारों की मौत ना हो जाए।
अखबारों की मौत होगी या नहीं, अगर अखबार बचेंगे तो उसकी क्या वजह होगी, इस पर चर्चा से पहले हमें अखबारों के मौजूदा कोरोना कालीन संकट पर एक नजर जरूर डाल लेना चाहिए। कोरोना संकट ने चूंकि समूची व्यवस्था को हिला रखा है, लिहाजा पूरी दुनिया में उपभोक्ता भी खुले हाथ से खर्च करने की बजाय बजत की पुरानी अवधारणा पर चल रहा है। उसे डर है कि पता नहीं कब, किस तरह के संकट का सामना करना पड़े। इसलिए वह हाथ खींचकर खर्च कर रहा है। जाहिर है कि इसका असर उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादकों और कारोबारियों की सोच पर भी पड़ा है। उन्हें पता है कि चूंकि ग्राहक पहले की तरह आना ही नहीं है, लिहाजा विज्ञापन देने का भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए विज्ञापनों में कमी आई है। चूंकि विज्ञापनों के सबसे बड़ा वाहक मीडिया ही है। मीडिया के चाहे जो भी रूप हों, विज्ञापन उसके पास कम आ रहा है। लेकिन कोरोना संकट में मजबूरी की महाबंदी में सबसे ज्यादा सांसत में अखबार हैं।
चूंकि महाबंदी के दौर में घरों में लोग रहने को मजबूर हुए, लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों मसलन टेलीविजन और इंटरनेट पर लोगों की आवक बढ़ी। चूंकि मीडिया के इन दोनों माध्यमों से शारीरिक संपर्क की गुंजाइश है ही नहीं, लिहाजा उन पर निर्भरता भी बढ़ी। लेकिन अखबार इसके ठीक उलट माध्यम है। अखबार पढ़ने के लिए उसे हाथ में लेना ही पड़ता है। इसलिए उसे कोरोना के विषाणु का आशंकित माध्यम तक मान लिया गया। इसकी वजह से अखबारों से ना सिर्फ उसके ग्राहक तक दूर होने लगे, बल्कि उसे घरों तक पहुंचाने वाले हॉकर भी। ऐसे में अखबारों का प्रसार घटा, प्रसार घटने और संकट की वजह से उपभोक्ता की बदली सोच के चलते अखबारों का विज्ञापन कम हुआ। इसकी वजह से अखबारों की कमाई घटी। अपेक्षाकृत कमजोर आर्थिक आधार वाले छोटे अखबारों की चिंता तो समझी जा सकती है, लेकिन इस स्थिति का फायदा बड़े अखबारों तक ने उठाने की ठान ली। अपने पृष्ठों पर सरकार और व्यवस्था को घेरने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की पैरवी करने वाले बड़े अखबारों का प्रबंधन और मालिकान तंत्र इस सोच को भुलाने में तत्काल जुट गया। जिन अखबारों का सालाना मुनाफा सैकड़ों करोड़ रुपये रहा हो, उन्होंने महज दो महीने के संकट में ही अपने उन साथियों को भगाने में देर नहीं लगाई, जिनकी बदौलत हाल के दिनों तक वे मोटा माल कूटते रहे थे। इन वजहों से माना जा रहा है कि अखबार मर जाएंगे।
चूंकि महाबंदी के दौर में लोग घरों में रहने को मजबूर हुए, लिहाजा उनकी निर्भरता इंटरनेट और टेलीविजन पर ज्यादा बढ़ी। इस वजह से अखबारों की वेबसाइटों के साथ ही उनके ई संस्करणों को भी लोगों ने पढ़ा। ई संस्करणों पर ग्राहकों की बढ़ती पहुंच ही है कि अब अखबार भी अपने ई संस्करण को मूल्य आधारित बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस हो या दैनिक जागरण या फिर अमर उजाला, इन अखबारों ने अपनी वेबसाइटों और ई संस्करणों तक पहुंच के लिए सब्सक्रिप्शन के विचार को आगे बढ़ा दिया है। चूंकि आने वाले दिनों में पांचवीं पीढ़ी के इंटरनेट की सुविधा बढ़ने वाली है, लिहाजा यह तो माना जा सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों के बाद तकनीक आधारित अखबारों के ई संस्करण पाठकों के प्रिय बनेंगे। इसके बावजूद अगर अखबार बचे रहेंगे तो उसकी बड़ी वजह अखबारों की अपनी जवाबदेही है।
सोशल मीडिया ने निश्चित तौर पर सूचनाओं तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाई है। लेकिन इसमें सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए जवाबदेही और संयम का अभाव है। दैनंदिन जीवन के बात-व्यवहार में आंखों के पानी का बड़ा महत्व रहा है। स्पष्टवादी और दुश्मन व्यक्ति भी कड़ी से कड़ी बात कहने के पहले कम से कम सामने वाले के उम्र, अनुभव और उससे अपने संबंधों का ध्यान रखता रहा है। अपराधी, आवारा और बदतमीज प्रकृति के लोगों का व्यवहार ही इसका अपवाद रहा है।
लेकिन सोशल मीडिया के मंच ने लोगों की आंख के पानी को सोख लिया है, आपसी संबंध और मानवीय मूल्यों को किनारे कर दिया है। अनपढ़ों, जाहिलों के मुहल्ले के झगड़ों, गांव के चट्टी-चौराहों के आवारा लोगों की भाषा और मूल्यों की तरह की भाषा भी सोशल मीडिया पर जमकर चलने लगी है। अपने निजी, वैचारिक और सामाजिक स्वार्थ के लिए झूठी और वास्तविकतारहित खबरों और विचारों की सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है। अच्छे और बुरे, दोनों तरह की ढेरों सामग्री सोशल मीडिया पर भरी पड़ी है। यह इतनी विविधरंगी है कि कई बार विवेकवान व्यक्ति भी उनमें कौन सही है और कौन गड़बड़, इसका आकलन करने और उसे समझने में चूक जाता है।
चूंकि पारंपरिक मीडिया में कई बार हकीकत की खबरों को भी प्रस्तुत करने या उसे रोकने के पीछे कई बार मीडिया संस्थान की नीतियां, विज्ञापनदाता का दबाव और सत्ता तंत्र के परोक्ष इशारे भी काम करते हैं। जबकि सोशल मीडिया इनसे दूर है। इस वजह से कमजोर एवं प्रताड़ित को सहारा देने, सच को सामने लाने के माध्यम के रूप में सोशल मीडिया की लोकप्रियता जरूर बढ़ी है। लेकिन जवाबदेही एवं मर्यादा के अभाव, फेक खबरों की भरमार ने इसकी गंभीरता को कमजोर भी किया है।
भारत के संदर्भ में देखें तो दो-तीन दशक पहले तक अखबारों की नीतियों को तय करने में उसके संपादक की भूमिका रहती थी। लेकिन अब संपादक नाम का प्राणी तो अतीत की वस्तु होता गया है। अब अखबारों की नीतियां उसके मालिकाना हक वाले कॉरपोरेट हाउस या उसके मालिक तय करते हैं। विज्ञापनदाता का दबाव और सत्ता तंत्र के परोक्ष इशारे संपादकीय विभाग को संचालित करते हैं। मार्केंटिंग टीम के टिप्स संपादकीय नीतियों में अक्सर आवाजाही करते रहते हैं। कुछ सच्चाइयां छिपाने के लिए सत्ता तंत्र अपने विज्ञापनों की भरमार कर देता है। दिल्ली में इन दिनों जमकर दिख रहा है। सत्ता तंत्र सीधे सच्चाई छुपाने के लिए धमकी ना देने की बजाय लुभावना विज्ञापनी बजट जारी कर देता है। इसके बावजूद अखबार को एक हद तक लोकोन्मुखी बने रहना होता है। क्योंकि अगर वह लोकोन्मुखी ना रहा तो लोक के रूप में उसके सामने पाठकों का जो बड़ा वर्ग होता है, उसे नकारने लगता है। जब वह तेजी से उसे नकारना शुरू करता है तो सत्ता तंत्र के लालची संकेत, विज्ञापनदाता के दबाव और मार्केटिंग विभाग का ज्ञान पीछे छूटने लगता है। ऐसे मौकों पर संपादकीय विभाग अपनी बातें भी रखने में सहज महसूस करता है। भारतीय संदर्भों में तो यह और ज्यादा प्रासंगिक है।
भारतीय पत्रकारिता का विकास स्वाधीनता आंदोलन की कोख से हुआ है, लिहाजा उसने आंदोलन के साथ की अपनी यात्रा में उसके कुछ मूल्य स्वीकार भी किए हैं। इसलिए अखबार एक सीमा के बाद ना तो फेक समाचार का समर्थन कर सकता है और ना ही दबाव तंत्र के आगे झुक सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में उसे जवाबदेह बने रहना पड़ता है। उसे विवेकवान भी रहना पड़ता है। विवेक और जवाबदेही की यह डोर ही अखबारों के लिए सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में उम्मीद की किरण है। अखबारों की बड़ी पूंजी उनके पाठक हैं और पाठकों की पूंजी उन्होंने अपनी जवाबदेही और विवेक के कारण हासिल की है। इसलिए अखबार जिंदा रहेंगे।
टेलीविजन में चूंकि तमाशा संस्कृति ज्यादा हावी है, लिहाजा वहां भी समाचारों की गंभीरता की गुंजाइश लगातार कम होती गई है। टेलीविजन का स्वरूप तमाशा और हंगामा के बीच विकसित हुआ है। इसलिए वह चाहकर भी इस तमाशा संस्कृति और हंगामेदार प्रवृत्ति को त्याग नहीं सकता। लेकिन अखबार के स्वभाव में भी ना तो हंगामा है और ना ही तमाशा। मार्शल मैक्लुहान ने कहा है, माध्यम ही संदेश है। अखबार शब्द का जिक्र आते ही विवेक और जवाबदेही का बिंब हमारे मन-मस्तिष्क में बनता है। यह बिंब ही अखबार की जिंदगी का उत्सकेंद्र हैं और प्राण वायु भी। अखबार जब तक इस उत्सकेंद्र को समझते रहेंगे, प्राणवायु को स्वीकार करते रहेंगे, जिंदा रहेंगे। हां, उनका स्वरूप, उनकी सज्जा जरूर बदल सकती है। ठीक वैसे ही, जब रेडियो की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने खुद को बदला, टेलीविजन की प्रतिद्वंद्विता में भी अपने को बचाए रखने के लिए अपनी लोकभूमिका को अस्वीकार ना करते हुए नई राह तलाशी। अखबार जिंदा रहेंगे, इसलिए भी कि कोरोना के संकट की गहराई को वे ही बताएंगे, वे इसे तमाशा नहीं बनाएंगे।
(नोटः यह आलेख उमेश चतुर्वेदी जी के फेसबुक वाल से साभार लिया गया है)
यह भी पढ़ें
मत बख्शों लॉकडाउन नियमों को तोड़ने वालों को
आत्महत्या कर रहे हताश-निराश-मजबूर मजदूरों को समझना-समझाना जरूरी
बिहार में बहार लाने की चुनौती
सियासत कीजिए लेकिन श्रमिकों के साथ नहीं
सियासत कीजिए लेकिन श्रमिकों के साथ नहीं